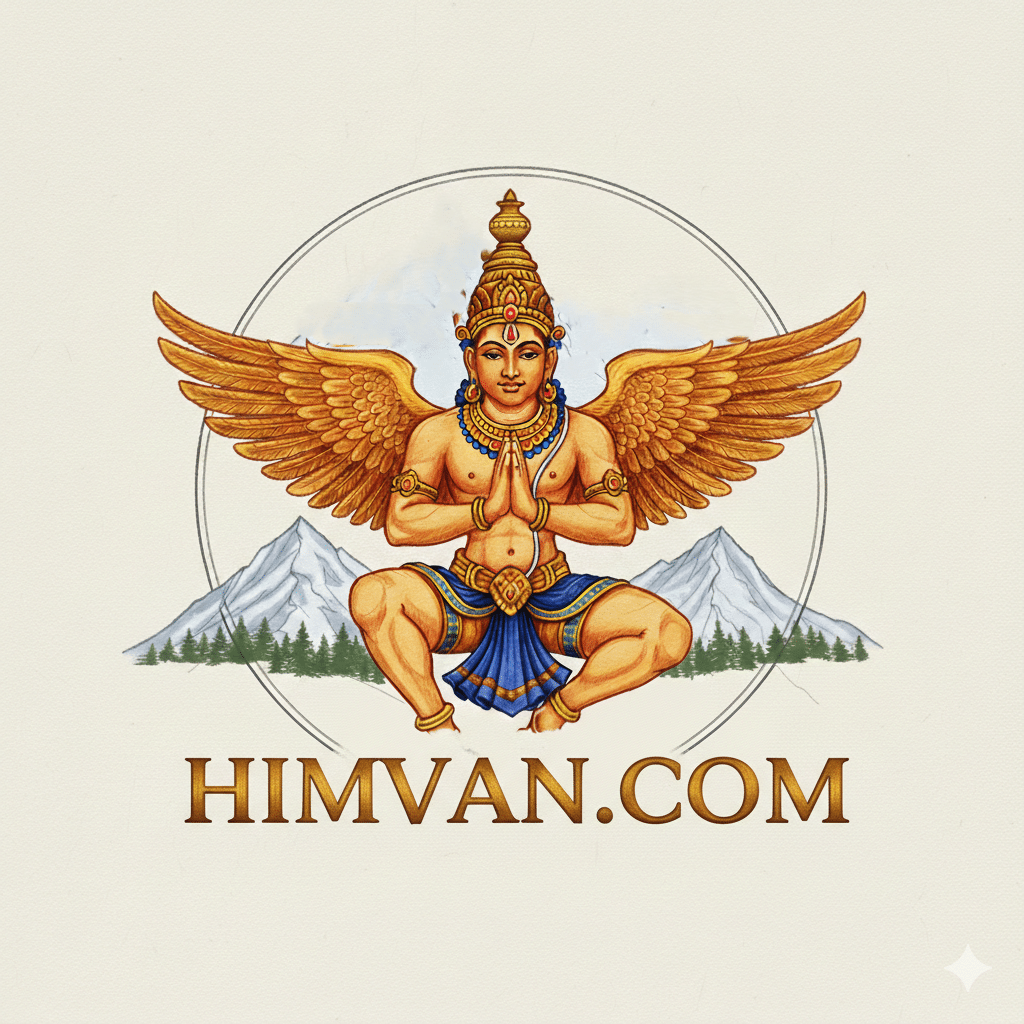उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में प्राचीन मंदिरोंके निर्माण की परम्परा लगभग सातवीं शती से निरन्तर पल्लवित होती रही है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण क्रमानुसार लकड़ी, ईंट तथा मजबूत पत्थरों इत्यादि से हुआ।

लकड़ी की प्रकृति दीर्घजीवी न होने के कारण काष्ठ निर्मित मंदिरों के निर्माण की परम्परा का अवसान सबसे पहले हुआ। इसके पश्चात अल्पमात्रा में ईटों के मंदिर बने और काल कवलित हो गये। तत्पश्चात सुदृढ़ पत्थर की शिलाओं से मंदिरों के बनानेका क्रम शुरू हुआ। पत्थरों की सुदृढ़ता तथा तकनीकी अनुकूलताके गुण के कारण तत्कालीन शिल्पियों ने तराशे गये पत्थरों से देवालय बनाने परम्परा को ग्रहण किया एवं उनके निर्माण में विभिन्न प्रवधियों को अपनाया।

पर्वतीय क्षेत्र में मंदिर अलग-अलग समय में विभिन्न आकार एवं शैलियों के बने। अधिकांश मंदिरों में निर्माण स्थल के पास के ही अत्यधिक कठोर पाषाण खंडों का उपयोग हुआ है। इनके निर्माण में मुख्यतः क्वार्टज, ग्रेनाइट, सिष्ट पत्थर का प्रयोग किया गया। ग्रेनाइट का प्रयोग सबसे अधिक हुआ । पर्वतीय क्षेत्र की आद्रता बहुल जलवायु पत्थरों पर विषम प्रभाव डालती है। बलुए पत्थरों में तो अत्यधिक छिद्रों की उपस्थिति के कारण इसका दुष्प्रभाव और भी अधिक होता है। आद्रता को अवशोषित करने के कारण बलुआ पत्थर अतिशीघ्र कमजोर हो जाता है। तत्कालीन शिल्पी इस तथ्य से भी भली-भांति भिज्ञ थे। जागेश्वर, बागेश्वर, नंदादेवी मंदिर अल्मोड़ा के अधिकांश मन्दिर क्वार्टज पत्थरों के बने हुए हैं। विद्वानों ने तो इन पत्थरों को अल्मोड़ा क्वार्टज का ही नाम दे दिया है।
इस क्षेत्र में काष्ठ का कपाट, छत्र तथा बिजौरे की निर्माण सामग्री के रूप में व्यापक प्रयोग हुआ। मंदिरों के बिजौरों की छत बनाने में देवदार की लकड़ी का ही प्रयोग सर्वाधिक हुआ। परन्तु नक्काशी की सुविधा के लिए तुन का भी व्यापक प्रयोग किया गया। कपाट निर्माण की सामग्री के रूप में भी देवदार की लकड़ी चुनी गयी। गढ़वाल के मंदिरों की काष्ठ सामग्री के रूप में देवदार, कैल और थुनेर भी प्रयोग की गयी है। देवदार की लकड़ी में दीमक इत्यादि का दुष्प्रभाव नगण्य ही होता है, यह लकडी शीघ्र खराब भी नहीं होती है। आज भी क्षेत्र में अलंकरणों के उत्कीर्णन के लिए तुन तथा देवदार से श्रेष्ठ व दीर्घायु कोई काष्ठ उपलब्ध नहीं है।

विष्णुधर्मोत्तर पुराण में उल्लेख मिलता है कि शिला निर्मित गृहों, दीवारों इत्यादि पर किसी न किसी प्रकार के लेप का प्रयोग निर्माण को चिरस्थायी बनाने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए ।
चूना अथवा सुधावर्ण का प्रासाद के सौन्दर्यकी अभिवृद्धि के लिए प्रयोग करने की सलाह भी दी गयी है।

चूने तथा मिट्टी का गारा बनाने का वर्णन भी हमें समरांगण सूत्रधार तथाअपराजितपृच्छा में मिलता है। इनके अनुसार बन्धन सामग्री को और अधिक स्थायी एवं मजबूत बनाने के लिए गेहूँ और जौ की भूसी तथा कठोर पत्थर के टुकडों का मिश्रण गारे में मिलाने की सलाह भी दी गई है। पुराविद एवं इतिहासकार डा० यशवंत्तसिंह कठोच ने वास्तुशिरोमणी नामक एक पांडुलिपि की खोज की है जो विक्रम संवत ।677 में रची गयी है। इसके अवलोकन से निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तरांचलमें भी वास्तुशिल्प की अपनी निश्चित परंपरा थी और स्थानीय वास्तुशिल्प का शास्त्रीय आधार पर विकास भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह गुप्त काल के बाद हुआ। अनेक विद्वानोंने तकनीक एवं निर्माण शैली के अनुसार हिमालयी शैली के पृथक अस्तित्व को स्वीकार किया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में यद्यपि मंदिरों की निर्माण सामग्री के विश्लेषण पर ज्यादा कार्य नहीं हुआ है इसलिए कहना जरा कठिन है कि निश्चित रूप से किन प्राकृतिक पदार्थों अथवा बहुलकों को प्रयोग स्थानीय देवालयों में किया गया होगा तो भी इस बात की प्रचुर संभावनायें मौजूद हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुतायत से प्राप्त वनस्पतियों एवं दालों का प्रयोग मंदिर निर्माण की प्रमुख सामग्री थी । पिसी मूंग अथवा उड़द की दाल का प्रयोग किये जाने की सम्भावनायें भी प्रचुर रूप से विद्यमान हैं। प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि दालों को पीस कर गारे में मिलाने से पलस्तर में जोड़ने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और पानी सोखने की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है।

सर्वमान्य तथ्य है कि वर्तमान के कृतिम बहुलक मिश्रित सीमेंट की वास्तु तकनीकी के मुकाबले प्राचीन समय में इस्तेमाल किये गये उड़द की दाल और तेलों का मिश्रण कहीं अधिक बेहतर था। प्रयोगों ने सिद्ध किया है कि प्राकृतिक बहुलक मिलाने से कंक्रीट में भी जोड़ने की क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाती है तथा पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन समय में प्रयोग में लायी गयी तकनीकी के कारण उस समय के स्मारक आज की सीमेंट तकनीकी से बने भवनों से कहीं अधिक मजबूत हैं।
पूर्व मध्यकाल में इस क्षेत्र के प्राचीन देवालय बिना गारे के भी निर्मित किये जाते थे। प्रस्तरखंडो को आपस में जोड़ने के लिए लोहे के आकुंड़ों का प्रयोग होता था। जागेश्वर व बमन सुआल मंदिर
समूह के पूर्व मध्यकालीन देवालय इसी प्रकार के बिना गारे की चिनाई से बनाये गये जिन्हें अन्दर की ओर से लौह आकुंड़ों से बांधा गया है। पूर्व मध्यकाल में इस क्षेत्र के प्राचीन देवालय बिना गारे के भी निर्मित किये जाते थे। प्रस्तरखंडो को आपस में जोड़ने के लिए लोहे के आकुंड़ों का प्रयोग होता था। जागेश्वर व बमन सुआल मंदिर समूह के पूर्व मध्यकालीन देवालय इसी प्रकार के बिना गारे की चिनाई से बनाये गये जिन्हें अन्दर की ओर से लौह आकुंड़ों से बांधा गया है।

पूर्व मध्यकाल में मंदिर विशाल बनाये गये। इस काल में लघु मंदिर भी विशाल
शिलाओं से बनाये गये जबकि उत्तर मध्यकाल के बाद विशाल मंदिरों में भी छोटे-छोटे प्रस्तरखंडों का उपयोग किया गया। पूर्व मध्यकाल में इन मंदिरों में केवल गर्भगृह या अन्तराल ही बनाया जाता था जिसे प्रारम्भ से ही अलग-अलग संरचनाओं में न बनाकर एक साथ ही बनाया जाता था। इनमें शिखर शीर्ष तथा केन्द्रीय भार को संतुलित किया जाता था। शिखर पर आरूढ़ चन्द्रिका इसको सम्बल प्रदान करती थी। मंदिर में गुरूत्व का निर्धारण इस प्रकार से होता था कि समूचे मंदिर का केन्द्र एकीकृत हो जाये जिससे यह मंदिर अधिकतम भूकम्परोधी हो जाते
हैं। इससे भूकम्प के समय मंदिर का शिखर इस प्रकार से दोलन करता है कि वह धराशायी
नहीं होते। कठिनाई से ही उनका कोई जोड़ ढ़ीला होता है। लौह आंकुड़े इन पत्थरों को मजबूती से बांधे रखतेहैं। ’
अवलोकन में यह तथ्य भी आया है कि शुष्क चुनाई से बनाये गये प्रासादों पर
समय अपना विपरीत प्रभाव अपेक्षया कम डाल पाया है जबकि मध्यकाल के बाद गारा
प्रयोग किये गये देवालय अपेक्षया शीघ्र जर्जर हो गये हैं। जिन मंदिरों में गर्भगृह, अन्तराल तथा मंडप एक साथ निर्मित किये गये उन्हें भी समय ने कम क्षतिग्रस्त किया है जबकि जिनमें गर्भगृह, अन्तराल और अर्धमंडप इत्यादि अलग-अलग करके बनाये गये उनके जोड़ सरलता से खुल गये।

मंदिरों के अवसान की प्रक्रिया या तो उनके प्रवेशद्वार से अथवा उनके शिखर से शुरू होती है। ऐसे मंदिरों में जोड़ ढीले होने से ललाटबिम्ब की शिलायें अपने स्थान से खिसक जाती हैं जिसके कारण मंदिरों के शिखर टेढ़े होने लगते हैं। कपिलेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा का शिखर इसी प्रकार टेढ़ा हुआ था।
मंदिरों में मिट्टी का गारा ही प्रयोग किया गया है। इस गारे में बंधनरूप में बाबिला जैसी घास का भी प्रयोग आश्चर्य की बात नहीं थी। कीटाणु रोधक रूप में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संगुण जैसी वनस्पतियां प्रयोग की गयीं। राख, और रेत के बारीक मिश्रण के प्रयोग की सम्भावना भी है। बाद में यही प्रवधियां बड़ी अट्टालिकाओं के निर्माण में भी प्रयोग की गयीं। परन्तु अभी मसाले और तकनीकी के सम्बन्ध में किसी निश्चय पहुंचने के लिए कार्य प्रारम्भ करने एवं उसका विश्लेषण शेष है।

आश्चर्य की बात यह है कि देवालयों की नींव भी अधिक गहरी नहीं डाली गयी। लेकिन यह जरूर है कि विशाल शिलाओं से अत्यधिक भारित कर दिया गया है। यह शिलायें भी इस प्रकार आपस में बंधी हैं कि भूगर्भीय हलचलों सहजतापूर्वक सहन कर लेती हैं।
एक तथ्य यह है कि नागर शैली के रेखा शिखर पीढ़ा शैली के शिखरों के सापेक्ष अपेक्षया कम क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनका कारण शिखर अन्दर की ओर बेडौल पत्थरों से अत्यधिक भारित कर देना रहा। सम्भवतः इसीलिए पीढ़ा शैली के बाद रेखा शिखर शैली शिल्पियों की प्राथमिकता बन गई। मंदिरों के पत्थरों को शिल्पियों ने लौह आंकुड़ों का भी प्रयोग किया परन्तु इन लौह आंकुड़ों में ऐसा कोई पदार्थ लेपित नहीं किया कि वे मोर्चा लगने से बच पार्ती। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में लौह आंकुड़ों में मोर्चा लगने के कारण वे न केवल स्वयं कमजोर हो जाते हैं वरन वे प्रस्तर खंडों में एक बल भी उत्पन्न करने लगते हैं जिसके कारण पत्थर टूटने लगते हैं। वर्तमान में ने इस समस्या से बचने के लिए तांबा अथवा निकिल प्लेटिंगयुक्त छड़ों का प्रयोग शुरू किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्र के प्राचीन स्मारको पर जलवायु कारकों के कारण फाइकस प्रजातियां, इराग्रेस्ट्रीला जैसी घास, फ्यूनेरिया , चिलमोड़ा, एस्पेंलनियम, क्रस्टोज लाइकेन, पौलीपोरस तथा नील-हरित शैवाल की विभिन्न प्रजातियांअधिकतर जड़ें जमा लेती है। पीपल, बेडू तो देवालयों के पत्थरों की संधियों में आम तौर पर उग आने वाले वृक्ष हैं। सर्वेक्षण में यह तथ्य भी आया है कि शैव परम्परा के देवालयों का नदियों के किनारे स्थापित किया जाना अत्यधिक प्रचलित था । नदियों के कारण आद्रता का मंदिर की नींव में पहुंचना सरल हो जाता है। आद्रता का मंदिर तक पहुंचने के लिए नदी की ओर से तटरक्षक बन्धों का निर्माण अवश्य किया जाना चाहिये जैसा कि कपिलेश्वर, बैजनाथ तथा बागेश्वर मंदिरों में किया गया।
अब यह समय की आवश्यकता है कि पर्वतीय क्षेत्र में देवालयों की निर्माण सामग्री के विश्लेषण पर भी कार्य किया जाये तभी हम देवालयों के रूप में मिली अपनी महान धरोहर के संरक्षण के लिए बेहतर कार्य कर पाने में सक्षम हो सकेंगे।